
विनीत कुमार, दिल्ली :
मीडिया और सांस्कृतिक अध्ययन (मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज) के जितने भी स्कूल हैं, इस क्षेत्र में जिन बड़े सिद्धांतकारों का नाम लिया जाता है, लगभग सबों ने माध्यम और तकनीक के रिश्ते को समझने और विश्लेषित करने का काम विस्तार से किया है। उनकी बहस का सिरा मोटे तौर पर दो तरफ खुलता है- एक तो ये कि तकनीक यदि मानवीय संवेदना और विचारों का विस्तार करती है तब तो इसका प्रसार और अपनाया जाना ज़रूरी है और यदि हमारी संवेदना को जड़, समझ को भोथरा और अभिव्यक्ति को स्टीरियोटाइप में बदल देती है। ऐसे में इससे दूरी बनायी जानी चाहिए। चूंकि तकनीक प्रसार और पहुंच के स्तर पर मानवीय संवेदना और अभिव्यक्ति को ऐसे ठिकानों तक ले जाती है जहां कि पारंपरिक संस्कृति और उत्पादन के तरीके से संभव नहीं है तो ऐसे में कुछ और नहीं तो भी लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार होता है और संप्रेषण के संसाधनों की पहुंच उनलोगों तक भी हो पाती है, जो पारंपरिक सांस्कृतिक चिन्हों ( कल्चरल कोड) को बरतने की स्थिति में नहीं होते। संस्कृति का यह रूप पॉपुलर संस्कृति के रूप में उनके बीच मौजूद रहता है।
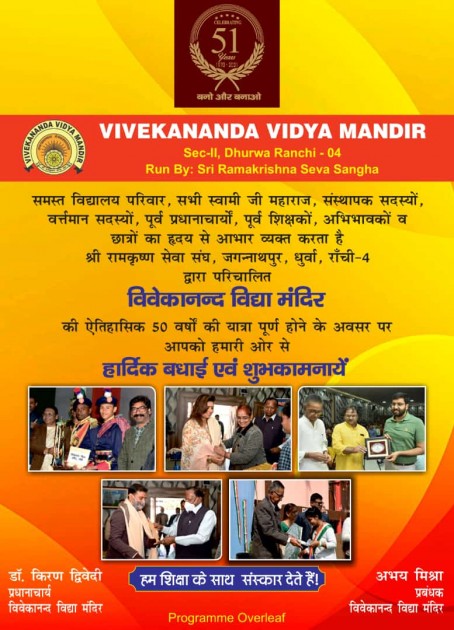
आप मार्शल मैक्लूहन की किताब "Understanding Media: The Extensions of Man"( 1964 ) पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो पूरी बहस इसी सिरे से खड़ी करते हैं कि माध्यम मानवीय संवेदना और विचारों का विस्तार करती है नहीं? अब ये अपने आपमें कितना दिलचस्प है कि सारे माध्यम तकनीक आधारित होते हैं लेकिन वो प्रिंट और रेडियो को ठंडा माध्यम बताते हैं जबकि टेलिविज़न को गरम माध्यम। ठंडा माध्यम का मतलब जो हमारी भावना, विचार, कल्पनाशीलता और संवेदना को विस्तार देने का काम करे और जो इससे ठीक उलट उससे नष्ट कर हम पर हावी हो जाए। वो बताते हैं कि प्रिंट और रेडियो हमारे भीतर समानांतर ढंग से भाव, विचार और कल्पनाशीलता का विस्तार करते हैं जबकि टेलिविज़न हम पर हावी होकर हमारे भीतर की कल्पनाशीलता और संवेदना को नष्ट करने का काम करता है। मैक्लूहन की इस अवधारणा और तर्क का आगे चलकर खंडन हुआ लेकिन आज भी आप बिना उनके इस तर्क को पढ़े बिना माध्यम और तकनीक के रिश्ते को ठीक-ठीक नहीं समझ सकते। रेमंड विलियम्स ने तकनीक, संस्कृति और माध्यम के आपसी रिश्ते को इसी आधार पर समझने का प्रयास किया कि वो मनुष्यों के साथ क्या करते हैं और फिर मनुष्य इसके साथ अपना संबंध किस रूप में बनाता है ? उनके हिसाब से चूंकि तकनीक मनुष्य निर्मित सुविधा और तंत्र है इसलिए वो चाहे तो इसे लगातार अपने पक्ष में बनाए रख सकता है. उनकी मशहूर किताब"Television: Technology and Cultural Form"( 1974) वो ज़रूरी किताब है जो कि मीडिया और सांस्कृतिक अध्ययन के छात्रों के लिए मनोहर पोथी है जिससे गुज़रते हुए वो आगे काफी कुछ सीख समझ सकते हैं।

बॉल्टर बेंजामिन का एक लंबा लेख है- The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction( 1935 ) जिसमें कि वो तकनीक और ख़ासतौर पर फोटोग्राफी और सिनेमा के माध्यम से संस्कृति के लोकतांत्रिक स्वरूप में ढलने की बात करते हैं और इस लिहाज़ से उसे वो बेहतर और ज़रूरी मानते हैं। आप जब इस लेख को पढ़ रहे होंगे तो दुनियाभर के उन संदर्भों का ध्यान हो आएगा जिनमें कि संस्कृति का एक उच्चतम रूप( High Culture )खड़ा करके समाज के बड़े वर्ग को इससे एकदम अलग-थलग रखा गया। उन्हें इस लायक माना ही नहीं गया कि वो सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध हो सकते हैं और उनकी हैसियत इन्हें बरतने की होगी। सांस्कृति अध्ययन के क्षेत्र में इसे बौद्रिआं का कैपिटल सी( "C") के अन्तर्गत विश्लेषित किया जाता है। जिस तरह हम समाजशास्त्रीय स्तर पर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ते हैं, सांस्कृतिक स्तर पर भी ऐसे वर्ग तैयार होते हैं और संघर्ष चलते रहते हैं. इस बात को समझने के लिए मौक़ा मिले तो जॉन ए. वीवर. की किताब "Popular Culture Primer"( 2009 ) पढ़िएगा. आप जान सकेंगे कि कैसे म्यूजियम जो कि किसी भी देश के सांस्कृतिक चिन्हों को समझने के लिए ज़रूरी संदर्भ होते हैं, उन्हें इस तर्क के साथ बंद किया गया कि लोगों में इसे एक्सेस करने की तमीज़ नहीं है और बाद में इसके जवाब में जब फिल्म की शक्ल में म्यूजियम लोगों के सामने आया तो एक बड़े वर्ग के लिए जाकर म्यूजियम देखने में दिलचस्पी ख़त्म हो गयी और एक लोकतांत्रिक परिवेश बनने में मदद मिली।

मैं इन सिद्धांतों और तर्कों के बीच जब सोशल मीडिया और उनकी गतिविधियों से गुज़रता हूं तो इस सिरे से भी विचार करता हूं कि हम तकनीकी सुविधा के बीच अपनी भाषा के साथ क्या कर रहे हैं और कहीं हमारी अभिव्यक्ति, मानवीय संवेदना और आपसी मानवीय रिश्ते इतने यांत्रिक तो नहीं हो गए कि हम महज लिखने के लिए लिख दे रहे हैं, बोलने के लिए बोल दे रहे हैं या सचमुच ऐसा करते हुए हम भावनात्मक स्तर पर समृद्ध हो रहे हैं। हमारे भीतर एक भराव आ रहा है और वैचारिकी के स्तर पर भी पहले से और सम्पन्न हो रहे हैं ? आप और हम जब इस सिरे से सोचना शुरु करते हैं तो हमसे जुड़नेवाले लोग महज एक संख्या और सब मिलकर एक ठसक नहीं होते कि हम इस संख्या के बूते धौंस जमाने की मुद्रा में आ जाएं और न ही तब इस्तेमाल किए गए शब्द कंकड़-पत्थर कि राह चलते हुए मौज में चटका गए। यदि ऐसा होता है तो हम और हमारे भीतर तकनीक यांत्रिकता आ गयी है और हम अपने जीने और व्यवहार करके से बिल्कुल अलग छिटक गए हैं। हमारे लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग, एक-दूसरे के लिखे पर टिप्पणी करने, शुभकामना संदेश लिखने और अपनी बात साझा करनेवाले हाड-मांस के वो लोग हैं जिनके सामने न होने पर भी हम उन्हें महसूस कर पाते हैं. जब ये महसूस होना बंद हो जाय और हम संख्या बल के प्रभाव में आने लग जाय तो समझ लेना चाहिए कि हम पर तकनीक हावी हो गयी है और ये मानवीयता का विस्तार होने के बजाय एक दूसरे कारोबार की तरफ मुड गया है. हमे ख़ुद को इस सिरे से सोचते रहने की ज़रूरत होती है।

आपलोगों ने मुझे मेरे जन्मदिन पर लगातार बधाई संदेश भेजे। मेरी और मेरे दोस्तों की टाइमलाइन पर भी लिखा। आधी रात गए मुझे मेरी इसी समझ ने इस बात के लिए तैयार किया कि जिस किसी ने भी तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हारे सिरे से यांत्रिक नहीं होना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि जो तुम्हारे सुंदर जीवन और भविष्य की कामना कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करो. लिहाजा, मैंने एक-एक करके सबके लिए कुछ-कुछ टिप्पणी करते हुए लिखना शुरू किया। ऐसा मैंने तक़रीबन डेढ़ सौ लोगों को किया होगा। आगे और भी करता कि फेसबुक ने कमेंट करने की सुविधा मेरे लिए बंद कर दी। मेरे पास यह संदेश आया कि आपके लिए यह सुविधा अस्थायी रूप से रोक दी गयी है। स्थिति ये बनी कि मैं किसी के लिखे पर कोई कमेंट नहीं कर सकता।रोज़मर्रा की बहस, असहमति, झगड़े, बहस और तंज़ के बीच कल की शुभकामनाओं के लिए मेरे मन तमाम लोगों के लिए सम्मान, स्नेह और प्यार है। आप एक-एक व्यक्ति के लिए मेरे भीतर आभार के शब्द हैं लेकिन उसे यहां फिलहाल लिखा नहीं जा सकता। वजह वो तकनीक और उसके साथ वो जुड़ी शर्तें जहां हमारी अतिसक्रियता हमें शक़ के घेरे में लाती है कि ये शख़्स असामान्य तो नहीं, एक साथ इतने कमेंट कर रहा है, इसकी हरकतें सामान्य तो नहीं ? अब देखिए कि तकनीक की उपलब्धता और उसके विस्तार के बीच यकायक एक ऐसा घेरा तैयार है जो हमें सीमित कर देता है। इस दायरे के आगे हमारी भावना और संवेदना पीछे छूटती, पस्त जान पड़ती है। हमारे पास दूसरे-तीसरे विकल्प न हों और ये समझ भी छूटती चली जाए कि हर कमेंट एक संख्या न होकर, हांड-मांस के इंसान के शब्द हैं तो सोचिए कि हम कैसी एक बंजर, ऊसर और बेस्वाद अभिव्यक्ति की दुनिया में जी रहे होंगे जहां शब्द शोर और वाक्य कोलाहल बनकर टकराते रहेंगे और हम उनसे कोई जुड़ाव महसूस न कर सकेंगे।
मैं फ़िलहाल इस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि पक्के तौर पर यह राय क़ायम कर सकूं कि तकनीक मानवीय संवेदना का विस्तार करती हैं या नहीं और न ही मेरा अध्ययन इतना गहरा है कि तय कर सकूं कि मानवीय आदतें तकनीक को अपनी ज़रूरत और सुविधानुसार नियंत्रित कर सकते। फ़िलहाल मैं बस इतनी कोशिश में रहता हूं कि हमारे लिखे और बोले गए शब्द महज संख्या में तब्दील न हो और न ही वो महज औपचारिकता में उलझकर यांत्रिक होते चले जाएं. ऐसा होने पर हमारा पूरा व्यवहार यांत्रिक होता चला जाएगा और हमारे भीतर महसूस करने की जो अद्भुत क्षमता है, वो कमजोर पड़ती चली जाएगी।

(लेखक दिल्ली के एक कॉलेज में प्राध्यापक हैं। मीडिया-विश्लेषक के रूप में मशहूर हैं। इश्क कोई न्यूज नहीं और मंडी में मीडिया उनकी दो चर्चित किताबें हैं।)
नोट: यह लेखक के निजी विचार हैं। द फॉलोअप का सहमत होना जरूरी नहीं। सहमति के विवेक के साथ असहमति के साहस का भी हम सम्मान करते हैं।