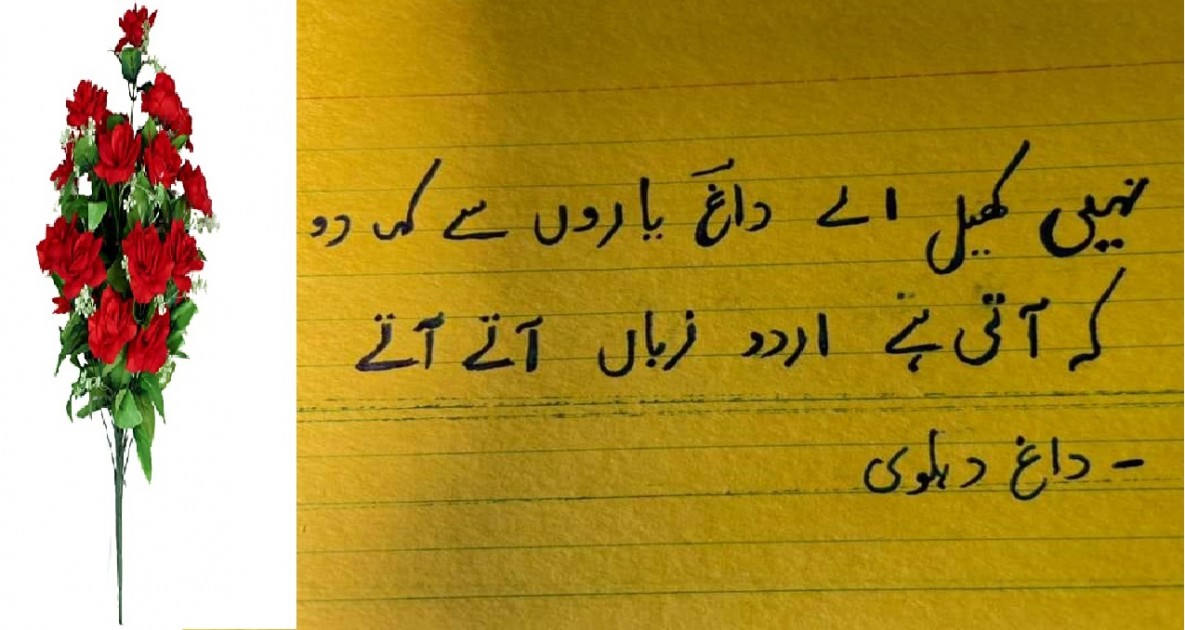
(उर्दू और हिंदी दोनों ठेठ भारतीय भाषाएं हैं। दोनों का उदय भी लगभग एक साथ ही हुआ। बाद में दोनों की राहें अलग-अलग हो गईं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रहे आनंद नारायण मुल्ला ने क्या खूब शेर कहा है, 'उर्दू और हिंदी में फ़र्क़ सिर्फ़ है इतना,हम देखते हैं ख़्वाब वो देखते हैं सपना।' हिंदी के प्राध्यापक और लेखक विनीत कुमार इस संस्मरणात्मक लेख में बता रहे हैं कि उन्होंने उर्दू कैसे सीखी। साथ ही जु़बान की अहमियत से भी रूबरू करा रहे हैं। पढ़िये उर्दू दिवस पर दिन रेख़्ता की पहली कड़ी -संपादक)
विनीत कुमार, दिल्ली :
इश्क़ में बेइज़्जती भी ज़रूरी है। ऐसा भी होता है लेकिन हर वक़्त ऐसा नहीं होता कि आप जिसके इश्क़ में पड़े हों, वो वायलिन-गिटार पर आपकी पसंदीदा धुन छेड़ती/ छेड़ता रहे। बीच-बीच में बे-इज़्ज़ती का सिलसिला चलता रहता है और तब तक जब तक कि आप और वो सम पर न आएं. सम पर आना मतलब दोनों का अहं( इगो) मिलकर हम में बदल जाय. कबीर ने तो लिखा भी है:
कबीर यहु घर प्रेम का, ख़ाला का घर नाँहि।
सीस उतारै हाथि करि, सो पैठे घर माँहि॥
कई बार यह सिलसिला ज़िंदगी के आख़िरी दम तक जारी रहता है और संभवतः इसलिए अहं के साथ होने की स्थिति में कई बार इश्क़ पीछे छूट जाता है। बीच-बीच में बे-ईज़्जत होते रहना पड़ता है। हां, फिर इसमें ये भी होता है कि सम पर लाने की कोशिश में आप इतने भी बे-ईज़्ज़त न होते चले जाओ कि अपनी ही नज़र में ईज़्ज़त चली जाय। सच में बहुत मुश्किल है इश्क़ करना, इश्क़ पाना और निभा ले जाना।
हम उर्दू के इश्क़ में पड़े और थोड़े बे-ईज़्ज़त हुए। अपनी तमाम तरह की पहचान और पीठ की गठरी उतारकर उर्दू की कक्षा में दाख़िल हुए। समय-समय पर बेईज़्ज़त हुए। ऐसा होने का सिलसिला और अनुभव सालों पहले बहुत पीछे रह गया तो सब अलग और नया लगा. लेकिन साथ में ये भी लगा कि सीखने के दौरान बेईज़्ज़त होना सच में बेहद ज़रूरी है और इश्क़ से ज़्यादा और किसकी पाठ इतनी मुश्किल है जिसकी सिलेबस तो इत्ती सी और अलग-अलग ढंग से दोहराने का काम आख़िर-आख़िर तक। ख़ैर।
कई बार उर्दू की कक्षा से हम आर्ट्स फैकल्टी, कमरा संख्या-12 से लौटकर अपने संस्थान या घर न जाकर रविकांत सर के पास जाते। जाते के साथ ही उर्दू लेकर बैठ जाते। वो अपना काम करते, मैं अपना काम। शुरु में तो सब ठीक रहा लेकिन थोड़े दिनों बाद वो देखने लगे कि मैं क्या लिख-पढ़ रहा हूं और फिर पूछने लगे- ये क्या लिखा है ? मैं कहता- कलीफा। उनके चेहरे का भाव एकदम से बदल जाता। एक बार कहा- यहां से फेंकूंगा तो सीधे बालकनी में गिरोगे।मुझे भीतर से हंसी छूट जाती और उन्हें भी समझ आता कि उन्होंने क्या कहा। हंस के सोशल मीडिया विशेषांक के दौरान संपादक काम हम साथ लेकर बैठते और कई बार मैं एकदम से अध्यापकीय मुद्रा में होता- तो, इसमें ये कैसे चला जाएगा ? कितने सारे पेपर, कितने सारे काम हमने एक साथ, बराबरी के साथ किए हैं लेकिन उर्दू के मामले में हम उनके आगे कहीं नहीं।
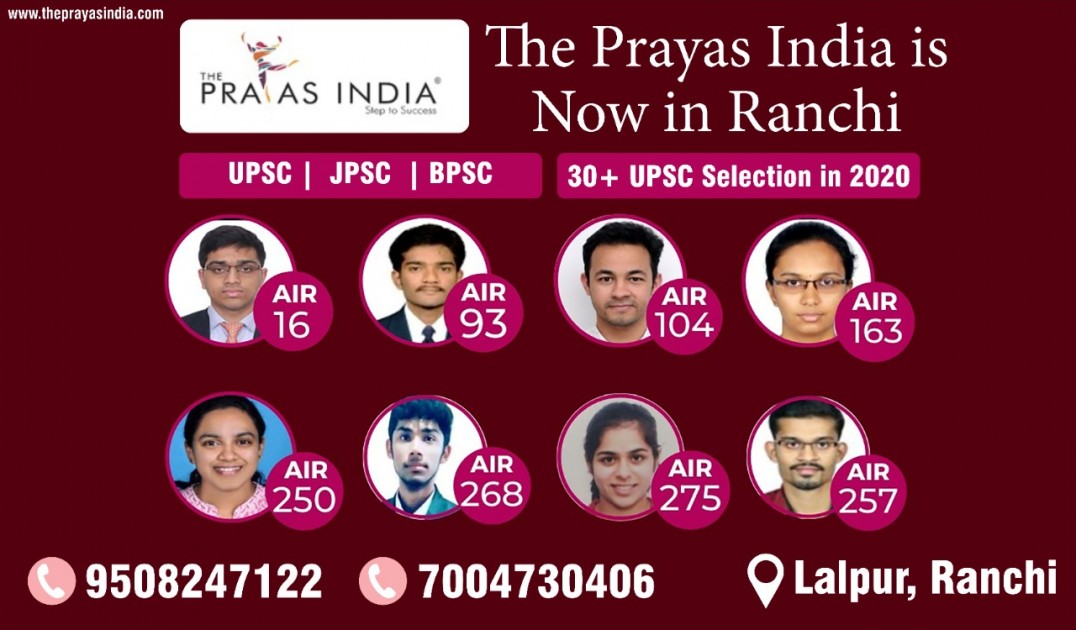
ये कांड हो जाने के बाद वो एकदम से अजीब भाव में आ जाते और कहते- चलो, चाय पीते हैं। उसके बाद कोई डांट-डपट नहीं. मैं चाय पीता, भीतर ही भीतर मुस्कराता और अपनी ये बेईज़्ज़ती बहुत प्यारी लगती। जिस ललक और उत्साह से उर्दू सीखना शुरू किया, आज लिखते हुए लगा कि ये मुझे पीछे छूट जा रही है। कई हर्फ़( शब्द ) लिखते हुए अटकने लगा, लिखावट छितरायी हुई सी लगने लगी। मैं भीतर से एकदम घबरा गया। उर्दू ऐसे तो नहीं छूट सकती। ऐसे कहां कुछ छूटता है. दाग़ साहब फिर से याद आए:
नहीं खेल ऐ 'दाग़' यारों से कह दो
कि आती है उर्दू ज़बाँ आते आते।
उर्दू बेहद ख़ूबसूरत ज़बाँ है। इतनी ख़ूबसूरत कि एक बार आप इसके इश्क़ में पड़ जाएं तो बाक़ी सब बेहद मामूली और फीका लगने लगे. कई लोग इससे इसलिए भी चिढ़ जाते हैं कि बहुत कोशिश के बावज़ूद भी बरत नहीं पाते और तब इसके साथ उल्टी-सीधी बातें जोड़ने लग जाते हैं। कुछ-कुछ वैसे ही, जैसे हम किसी के इश्क़ में हों और वो ज़िंदगी में शामिल न हो सके तो उसे लेकर उल्टी-सीधी बातें बनाने लग जाएं। ये इश्क़ तो नहीं. उर्दू न सीख सकें, बस वो इश्क़ बनाए रखें तब भी कितना कुछ अपने भीतर बचाए रख सकेंगे ऐसे लोग. इश्क़ के होने और अपने भीतर बचे रहने का एहसास भी कम तो नहीं ?

(लेखक दिल्ली के एक कॉलेज में प्राध्यापक हैं। मीडिया-विश्लेषक के रूप में मशहूर हैं। इश्क कोई न्यूज नहीं और मंडी में मीडिया उनकी दो चर्चित किताबें हैं।)
नोट: यह लेखक के निजी विचार हैं। द फॉलोअप का सहमत होना जरूरी नहीं। सहमति के विवेक के साथ असहमति के साहस का भी हम सम्मान करते हैं।